राजेन्द्र यादव होने का अर्थ-----प्रेमकुमार मणि
राजेन्द्र यादव होने का अर्थ
प्रेमकुमार मणि
28 अगस्त राजेन्द्र जी का जन्मदिन है. इसी तारीख को 1929 में उनका जन्म हुआ था. जब वह थे तब इस तारीख को दिल्ली और आसपास के खूब सारे लेखक, झस कर युवा लेखक, दिल्ली के किसी तय ठौर पर इकट्ठे होते थे और उनका जन्मदिन हर साल एक जलसे का रूप ले लेता था. याद कर सकता हूँ यह सिलसिला 1990 के कुछ पहले से शुरू हुआ और उनके जीवन के आख़िरी वर्ष तक चला. ज्यादातर जलसों में मैं शरीक होता था. लेकिन आखिरी साल मैं देहरादून में था और उनके जन्मदिन पर बधाई देने केलिए उन्हें फोन किया तब उन्होंने बच्चों जैसी जिद की; शाम तक किसी भी तरह चले आओ. मैंने कहा, अगले वर्ष रहूँगा, इस बार दूरभाषिक बधाई ही लीजिए. वह उदास हुए . आवाज में उतरी उनकी उदासी आज भी महसूस करता हूँ. कहा- अगला साल किसने देखा है. मैंने उनकी बात नहीं मानी और उसका अफ़सोस मुझे हमेशा रहेगा. अक्टूबर महीने में दिल्ली होते हुए ही पटना आया था. दिल्ली में रुका नहीं . कुछ समय बाद मुझे फिर दिल्ली जाना था. सोचा अगली दफा ही उनसे मिलूंगा. लेकिन जैसे ही पटना आया उसके हप्ता भर के भीतर ही एक सुबह उनकी मृत्यु की मनहूस खबर मिली. 28 अक्टूबर 2013 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया.
राजेन्द्र जी का होना केवल एक लेखक का होना नहीं था. उनके साथ उनकी एक अपनी दुनिया थी,जिसके अपने ही किस्से थे. वह किस्सागो तो थे और उनकी मुख्य पहचान भी यही थी; किन्तु इतना भर ही नहीं थे. बनते हुए राष्ट्र का वैचारिक आरोह - अवरोह उनके लेखन में आप ऐसे अंदाज़ में देखेंगे ,जैसा किसी दूसरे लेखक में नहीं है. आज़ादी के बाद हमारे हिंदी साहित्य में बहुत कुछ बदल रहा था. भारत गाँव बहुल देश था; किन्तु नगर चेतना का विस्तार राष्ट्रीय आंदोलन ने गहराई से कर दिया था. गाँव भी इस चेतना से आप्लावित हो रहे थे. आज़ादी के भाव, जनतंत्र के लिए उत्साह और सोचने का एक वैश्विक नजरिया सुदूर गाँवों तक फ़ैल रहा था. साम्प्रदायिकता के नाम पर जो देश का विभाजन और खून खराबे हुए थे सब को भूल कर लोग अपने वतन को संवारना चाहते थे. हजार तरह की मुश्किलें थी ,अनेक दकियानूसी विचार और उनके प्रचारक ख़म ठोक कर प्रगति की राह में खड़े थे. लेकिन गांधी और नेहरू के नाम की पताका लिए लोग नई दुनिया के सपने भी संवार रहे थे. 1950 के दशक में नेहरू सरकार ने सबसे अधिक जोर शिक्षा पर दिया था,खास कर प्राथमिक शिक्षा पर. गाँव -गाँव में स्कूल खुल रहे थे और उसमे सभी जाति -वर्ग और लिंग के लोग जा सकते थे. एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार ने निचले स्तर पर भी बराबरी की प्रबल भावना जगा दी थी.
आज़ादी की आंधी लगातार फैलती -पसरती जा रही थी. आज़ादी के इसी उल्लास का एक ब्यौरा फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास ' मैला आँचल ' में दिया है. एक पिछड़े हुए गांव; जहां बारहों बरन के लोग रहते हैं; का स्वाभाविक नायक एक जाति कुल- हीन प्रशांत बनता है. हालांकि इस बात में सच्चाई है कि सामान्य तौर पर भारतीय लेखकों ने आज़ादी के उन्मेष का प्रभावी चित्रण नहीं किया. कुछ यही वह समय था जब बंगला लेखक बुद्धदेव बासु ने लिखा था कि भारत ने यूरोप जैसी पीड़ा नहीं झेली इसलिए भारतीय लेखकों में दुःख के अनुभव का अभाव है और यह अभाव ही भारतीय साहित्य के औपन्यासिक दारिद्र्य का कारण है. यह विडंबना ही है कि किसी रचनाकार ने बासु को जवाब नहीं दिया,जवाब दिया समाजवादी राजनेता और चिन्तक राममनोहर लोहिया ने. बासु को जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि जिस बंगाल में भीषण अकाल और आज़ादी के दरम्यान दंगे -फसाद से लाखों लोग मारे गए ,तबाह हुए ,वहां के लेखक को यदि पीड़ा के अनुभव का अभाव है तो इसका मतलब साफ़ है कि हमारे देश में पीड़ा भोगने वाले और लिखने वाले अलग -अलग वर्गों से आते हैं. वे दो दुनिया दो राष्ट्र हैं. जो पीड़ा भोगते हैं ,वे लिखते नहीं, और जो लिखते हैं वे पीड़ा नहीं भोगते. हमारी हिंदी का हाल और बुरा था. हिंदी लेखक आम तौर पर समाज के द्विज वर्ग से ,ऊँची जातियों से आए थे. आज़ादी ने उनके कुछ विशेषाधिकार ख़त्म कर दिए थे. नए संविधान ने मनुष्य को जाति -गोत्र या धर्म के निकष पर नहीं, केवल मनुष्य होने के निकष पर देखा था. इन स्थितियों ने लेखकों की मानसिकता को अस्थिर और कुछ बेचैन कर कर दिया था. स्वाभाविक था इससे मुक्ति केलिए वे चिरंतन और शाश्वत की साधना में लग गए. दुर्भाग्य यह है कि आलोचकों ने भी इन स्थितियों की कभी सार्थक समीक्षा नहीं की.
लेकिन 1950 के दशक में मुट्ठी भर नौजवान लेखकों ने हिंदी साहित्य की इस शांत -गंभीर स्थिति को तोड़ने की कोशिश की . यह कार्य कविता विधा में होना असंभव था,क्योंकि वहाँ संवाद की स्थितियां विकसित होने की गुंजायश कम होती है. उपन्यास भी सामान्य जन की विधा नहीं हो सकती थी. इसकी संभावना कहानी में हो सकती थी. तीन दोस्तों ने मिल कर कहानी विधा के माध्यम से मध्य वर्ग से एक सार्थक साहित्यिक संवाद बनाने की कोशिश की और कुछ ही समय में यह नई कहानी आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया. इसके प्रस्तावक थे-- मोहन राकेश , राजेंद्र यादव और कमलेश्वर.
साहित्य में मानो एक भूचाल आ गया. आज़ादी का जो उन्मेष देश भर में फ़ैल रहा था,उसे गति मिली. गाँव -कस्बों की सामंती -पुरोहिती चेतना पर बिना किसी नारेबाजी के इन कहानियों ने चोट की. जीवन के प्रति स्थापित नजरिए को किंचित बदलने की कोशिश की. एक नई जुबान , कहन के एक विशिष्ट अंदाज़ को विकसित किया. सब मिला कर नेहरू के साइंटिफिक टेम्पर से साहित्य को चुपचाप नत्थी करने का प्रयास किया. नई कहानी एक आंदोलन बन गया. इससे रेणु भी जुड़े और निर्मल वर्मा भी , उषा प्रियंवदा और मन्नू भंडारी भी. प्रगतिशील आंदोलन की तरह यह कोई राजनीति प्रेरित आंदोलन नहीं था, साहित्यिक आंदोलन था.
नई कहानी आंदोलन ने ग्राम-कथा और प्रेमचंद की परंपरा के नाम पर चले आ रहे दुराग्रहों की अवहेलना की. स्वस्थ और आधुनिक जीवन-बोध की प्रस्तावना की ,जिसमें संकीर्णताओं केलिए कोई जगह नहीं थी. भाषा ,भाव और प्रतीकों को नए ढंग से संवारने की कोशिश की गई. इन लेखकों की यह चिंता भी थी कि हिंदी साहित्य को विश्व की अन्य जुबानों के बराबर रखना है. यह एक नई चुनौती थी. यह राष्ट्रीय-जागरण का नहीं, राष्ट्र-निर्माण का साहित्य था. ये तमाम युवा लेखक अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अवगत थे. संजीदगी के साथ उसका निर्वाहन भी कर कर रहे थे.
1970 के इर्द-गिर्द यह आंदोलन पझा चुका था. नई सामाजिक -राजनीतिक स्थितियों ने साहित्य के समक्ष नई चुनौतियाँ रखी थी और साहित्य इनसे अपनी तरह से निपट रहा था. इंदिरा गांधी के समाजवादी जुमलों और नक्सलबाड़ी के धधकते खेत-खलिहानों की चर्चाओं का यह दशक था. इसी दशक में राजेंद्र जी से मेरा परिचय हुआ. पहली दफा मिला तब मुल्क में राजनीतिक इमेर्जेंसी लगी हुई थी. दिल्ली के अपने दफ्तर में,जो तब उनके प्रकाशन का था, वह मिले थे. मुझे वह कुछ बनावटी- व्यक्तित्व के लगे. लेकिन दो तीन मुलाकातों के बाद हम सहज हुए और फिर तो लड़ने -झगड़ने भी लगे. उनके जैसा जनतांत्रिक व्यक्तित्व वाला इंसान मैंने बहुत कम देखा है. उनसे दुनिया भर की बातें होती थीं. कुछ मुद्दों पर मतभेद भी होते थे. कभी -कभार किसी बात पर रंज और क्षुब्ध भी होते,लेकिन उनकी रंजगी टिकने वाली नहीं होती थी. अपने व्यक्तित्व में वह बिल्लौर की तरह सुथरे और किसी बच्चे की तरह कोमल थे. मेरे साथ ही नहीं, किसी के साथ भी उनका ऐसा ही बर्ताव होता था. जब 1986 में उन्होंने 'हंस ' पत्रिका निकालना तय किया, तब मुझ से भी बात की. मैं उसकी सफलता को लेकर शंकित था. बिना किसी पूंजीवादी घराने के सहयोग से नियमित साहित्यिक पत्रिका निकालना कितना कठिन है, इसे वही समझ सकता है जिसने कभी इस दिशा में प्रयास किया हो. लेकिन जल्दी ही हंस की चर्चा देश भर में होने लगी. दरियागंज के अंसारी रोड में स्थित हंस का दफ्तर कुछ -कुछ वैसा ही साहित्यिक केंद्र बनता चला गया, जैसा पेरिस का गालीमार प्रकाशन जहाँ सार्त्र , कामू और सिमोन द बोउआ जैसे लेखक नियमित बैठते थे. कहीं पढ़ा था दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान हिटलर ने उस प्रकाशन हाउस को बम से उड़ा देने का खास निदेश दिया था. हंस का दफ्तर कुछ अर्थों में अपने समय का हिंदुस्तानी गालीमार बन चुका था. राजेंद्र जी द्वारा लिखे सम्पादकीय लेखों के पाठक देश भर में फैले थे. इन लेखों में उन्होंने केवल साहित्यिक सवालों को नहीं अपने समय के ज्वलंत सामाजिक -राजनीतिक सवालों पर भी टिप्पणियां की और कई दफा यथास्थितिवादी तत्वों के निशाने पर भी आए. अपने दौर के वह पहले लेखक थे, जिन पर उनके लेखों के लिए कई दफा और कई जगहों पर मुकदमे दायर किए गए. कई रूपों में वह समय अत्यंत चुनौतीपूर्ण था. इसी दौर में रामजन्मभूमि का मामला उभरा और हिंदुत्व की राजनीति को बल मिलने लगा. शाहबानो मसले पर कट्टरतावादी मुस्लिम मन भी जाग्रत हुआ. सती प्रथा के सवाल उठे, मंडलवाद के रूप में जातिवादी आग्रहों का तूफ़ान खड़ा हुआ. इस विषम माहौल में अनेक लेखक अपने दकियानूसी ख्यालों के साथ प्रकट हुए. कुछ ऐसे थे जिन्होंने इन सवालों से तटस्थ रह कर अपनी होशियारी दिखलाई. राजेंद्र यादव ने ऐसा नहीं किया. वह अपने समय के सवालों से जूझते -टकराते रहे . अपनी साहित्यिक पत्रिका को उन्होंने वैचारिक -विमर्श का खुला मंच बनने दिया. उनका हर सम्पादकीय किसी भी कथा-कविता से अधिक चर्चा में होता था.
वह अद्भुत लेखक थे. नौजवान लेखकों से घिरा होना उनकी खास फितरत होती थी. 1990 के बाद अपनी पत्रिका को स्त्री और दलित विमर्श केलिए उन्होंने समर्पित कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि हासिए के लोगों की चिंता जिस साहित्य और समाज को नहीं है , वह जनतांत्रिक समाज नहीं है. राजनीति उनकी पसंद का क्षेत्र कभी नहीं रहा, लेकिन राजनीतिक सवालों की उपेक्षा उन्होंने कभी नहीं की. उनकी चिंता केवल यह होती थी कि उनका हिंदी साहित्य अपनी चेतना में वैश्विक बने और हिंदी लेखकों को वह प्रतिष्ठा मिल सके, जो दूसरे विकसित जुबानों के लेखकों को मिलती है.
मैं यह नहीं कहूंगा कि हंस ने हमेशा यह तेवर बनाए रखा. ऐसा संभव नहीं था. पिछली सदी के अंतिम दशक में जब आर्थिक उदारीकरण का दौर आया तब राजनीति भी उससे प्रभावित हुई. सदी के आखिर तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दक्षिणपंथी ताकतें केंद्र में सरकार पर काबिज हो चुकी थी. आरम्भ में तो हंस और राजेंद्र यादव ने एक वैचारिक प्रतिपक्ष खड़ा करने की खूब कोशिश की ,लेकिन बाद में स्त्री और दलित -विमर्श के नाम पर मिथ्याचार भी विकसित होने लगे. अस्वस्थता के कारण राजेंद्र जी अब पहले जैसा नियंत्रण नहीं रख सकते थे. लेकिन दो दशकों तक राजेंद्र यादव ने हंस के माध्यम से हिंदी क्षेत्र में वैचारिक मशाल जलाए रखा और समाज को दृष्टि देते रहे. यह बड़ी बात है.उनके नेतृत्व में हिंदी साहित्य में एक नई वैज्ञानिक परिदृष्टि का उन्मेष हुआ. इसे रेखांकित करना बहुत मुश्किल नहीं है. राजेंद्र यादव का मतलब है आधुनिकता से लबरेज ऐसे विचारों का समाहार जहाँ स्वतंत्रता और मनुष्यता के नए अर्थ उभरते हैं. हिंदी की दुनिया उन्हें भला कैसे भूल सकती है.
--
प्रेमकुमार मणि
--------------------------------------------------------
#hanshindimagazine #hanspatrika #हंसपत्रिका #अगस्त2023 #august2023 #राजेन्द्रयादव #rajendrayadav #jayantivishesh #जयंतीविशेष #vishesh #rajendrayadavsamman #अपनेयुगकाखलनायक #apneyugkakhalnayak
-------------------------------------------------
सकारात्मक भारत -उदय आंदोलन -9वां वर्ष
Uday Manna
RJS PBH
संस्थापक
8368626368


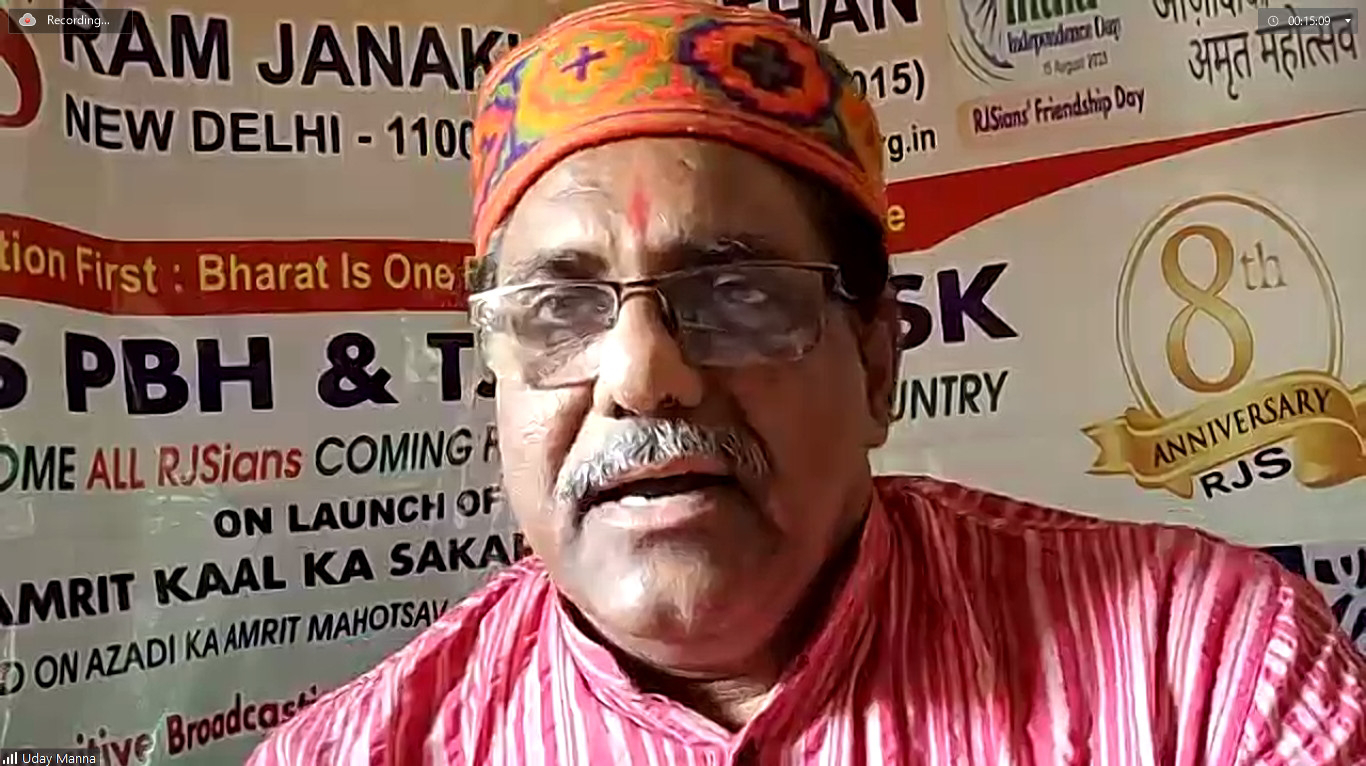



Comments
Post a Comment